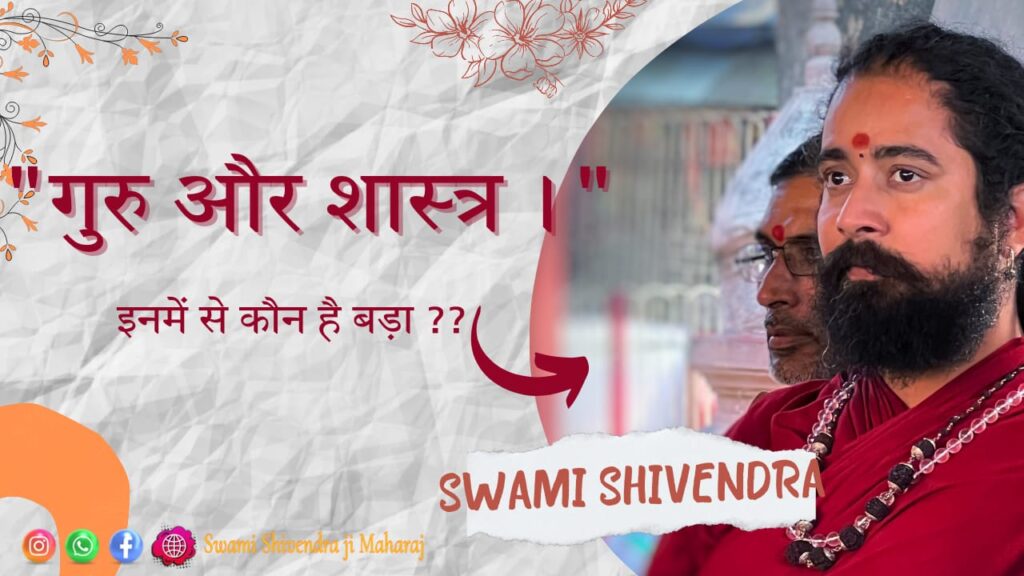“गुरु और शास्त्र ।”
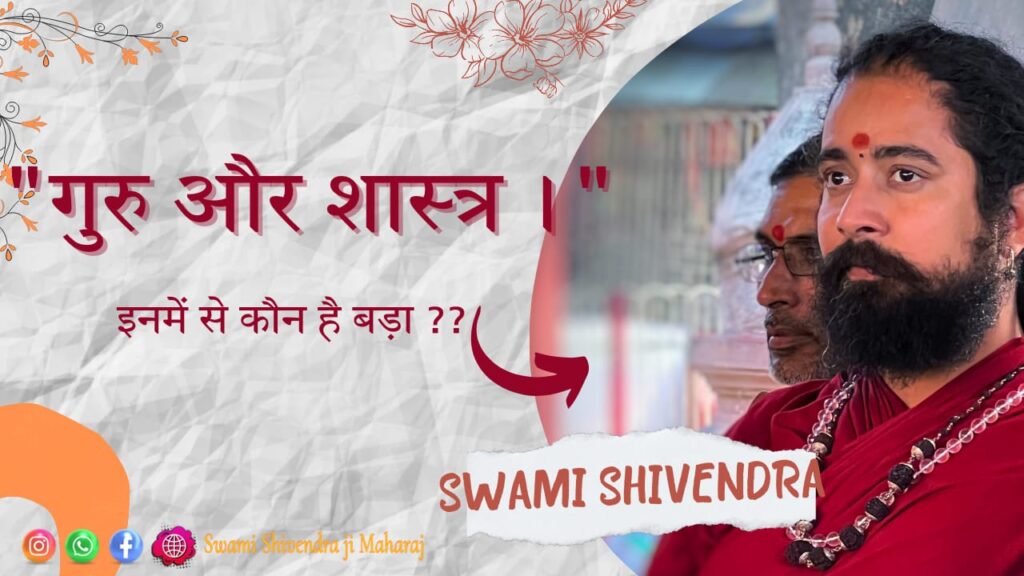
नारायण।
शास्त्र तो अनादि काल से मौजूद है, वह हमारा कल्याण कहाँ कर पाया। विचार करने पर पता लगता है कि हमें सद्गुरू मिले तभी हमारा कल्याण हुआ, अतः वे ही प्रधान हेतु हैं। सूर्य कमल को खिला तो देता है पर तभी जब कमल जल में हो , बाहर पड़े कमल को तो वह सुखा ही डालेगा। शिष्य भी गुरुसन्निधि में रहे तभी शास्न उसके अज्ञान को मिटायेगा, गुरु के बिना तो शास्त्र और ज्यादा उलझन का हेतु बन जायेगा। अतः अध्यात्मसाधक को सद्गुरु का ही समाश्रयण लेना चाहिये। गुरु के पास रहे, सेवा करे तभी गुरु उसकी योग्यता की जाँच कर पायेगा। गुरु जो निर्विशेष तत्त्व समझाते हैं उसे ग्रहण करना चाहता भी है या नहीं – यह गुरु को तभी मालूम पड़ेगा जब शिष्य निकट रहेगा।
हर व्यक्ति दीर्घ काल तक स्थूल शरीर से नहीं भी निकट रह पाये तो भी उसे मन से गुरुचिन्तन करते रहना चाहिये जैसे माता दूर होने पर भी पुत्र का चिन्तन करती है। शिष्य का मन सांसारिक वस्तुओं में न लगे यह जरूरी है, अतः गुरू के चरणकमलों में मन लगाये रखना चाहिये। शरीर से भी उनकी आज्ञाओं का पालन अर्थात् धर्म करते रहना चाहिये। गुरु की शिक्षा का पूर्ण तत्परता से पालन करना ही उनकी मुख्य उपासना है। जैसे चिड़ियों के चूजें खुद नहीं खा सकते, चिड़िया हीं उनके मुँह में डाले तो खाते हैं ऐसे हम स्वयं शास्त्ररहस्य नहीं समझ सकते, आचार्य ही समझाये तो हमें पता चल सकता है। अतः स्वयं के भरोसे न रहकर आचार्य की महत्ता याद रख उन्हीं की शरण में रहना चाहिये।
गुरु के प्रति समर्पण का प्रसिद्ध दृष्टान्त छत्रपति शिवाजी हैं। उन्होंने समर्थ गुर श्रीरामदासजी को अपना सारा राज्य अर्पित कर दिया, फिर उन्हीं की आज्ञा से केवल व्यवस्थापक की हैसियत रखकर राज्य की संभाल करते रहे। अतएव उन्होंने अपने राज्य का ध्वज भी भगवे रंग का रखा था क्योंकि राज्य तो गुरु का, महात्मा का था। यों अपने” स्व” का समर्पण करने पर ही गुरु का पूर्ण नियन्त्रण शिष्य पर रहता है जिससे शिष्य वही बन जाता है जो गुरु है। जैसे मरणासन्न रोगी वैद्य से शास्त्रार्थ नहीं करता, जो दवा वह बताये उसे जल्द से जल्द लेता है, वैसे ही संसारताप से तप्त शिष्य को गुरु का उपदेश शीघ्रातिशीघ्र अपने जीवन में उतारना चाहिये, ऊहापोह में ही इतना समय न गंवा दे कि साधना करने की अवस्था ही बीत जाये। अपनी योग्यतानुसार ही शिष्य समझ पायेगा अतः ज़रूरी नहीं कि वह शास्त्र का विद्वान् बन सके लेकिन शास्त्रोक्त साधन अपना कर स्वयं का कल्याण तो कर ही सकता है। अतः जैसे रोगी खुद वैद्य बनकर दवा नहीं लेना चाहता वरन् उपलब्ध वैद्य से पूछकर दवा लेकर ठीक होना चाहता है, ऐसे शिष्य यह न सोचे कि पूरा शास्त्र समझकर साधना करूँगा, वरन् गुरु जैसा बताये वैसे साधन में लग जाये। चिड़िया का बच्चा खुद दाना नहीं ले पाता, चिड़िया ही उसे खिलाती है, इसी प्रकार साधक अपने लिये उपयोगी साधन नहीं ढूँढ सकता, गुरु ही उसे उसके योग्य साधन बताते हैं। शिष्य को परमेश्वरप्राप्ति हो तभी गुरु अपनी सफलता समझता है। अतः परमेश्वर को प्राप्त करना चाहे तो शिष्य को गुरु के प्रति समर्पण रखना ही उचित है।
क्योंकि गुरु शास्त्रानुसारी ही उपदेश देता है इसलिये शिष्य को समझते हुए उसके पालन का मौका रहता है। गुरु की बात माननी तो है, पर साथ ही साथ समझनी भी है। यदि विचार से दूर रहेगा तो केवल अक्षरशः आज्ञा पालन से परम कल्याण नहीं प्राप्त कर पायेगा। किसी के घर बिल्ली पाली हुई थी। श्रद्धादि के समय वह बीच में न आ जाये, अतः पिता कहते थे” बिल्ली बाँध दो तब कर्म प्रारम्भ करें।” पुत्र आज्ञाकारी तो थे, समझदार नहीं थे। पिता जी मर गये। कुछ दिनों में बिल्ली भी मर गयी। अब पुत्र नयी बिल्ली लाये क्योंकि बिल्ली बाँध बिना श्राद्ध कैसे होगा? विचारहीन व्यक्ति इसी प्रकार गुरु की आज्ञा का भाव समझ नहीं पाते। अतः शिष्य विनम्रता पूर्वक पूछे, समझने की कोशिश करे, यह जरूरी है पर समझने से पूर्व ही उनकी आज्ञा का पालन तो प्रारम्भ कर ही दे। जैसे दृश्य को आँखों की सीध में ले जायें तो आपकी आँख में उसका चित्र बनना कोई मुश्किल नहीं होता ऐसे ही आचार्य से शिष्य का समीचीन संबंध बन जाये तो न गुरु को वन शिष्य को कोई मुश्किल पड़ती है, आराम से शिष्य परमेश्वर का दर्शन पा लेता है। नाली बनाने का परिश्रम कर दें तो नहर से खेत में पानी स्वतः आ जाता है, गुरु सेवा का भी परिश्रम कर लें तो गुरु में जो परमात्मज्ञान है वह स्वतः आपके हृदय में उतर आयेगा।